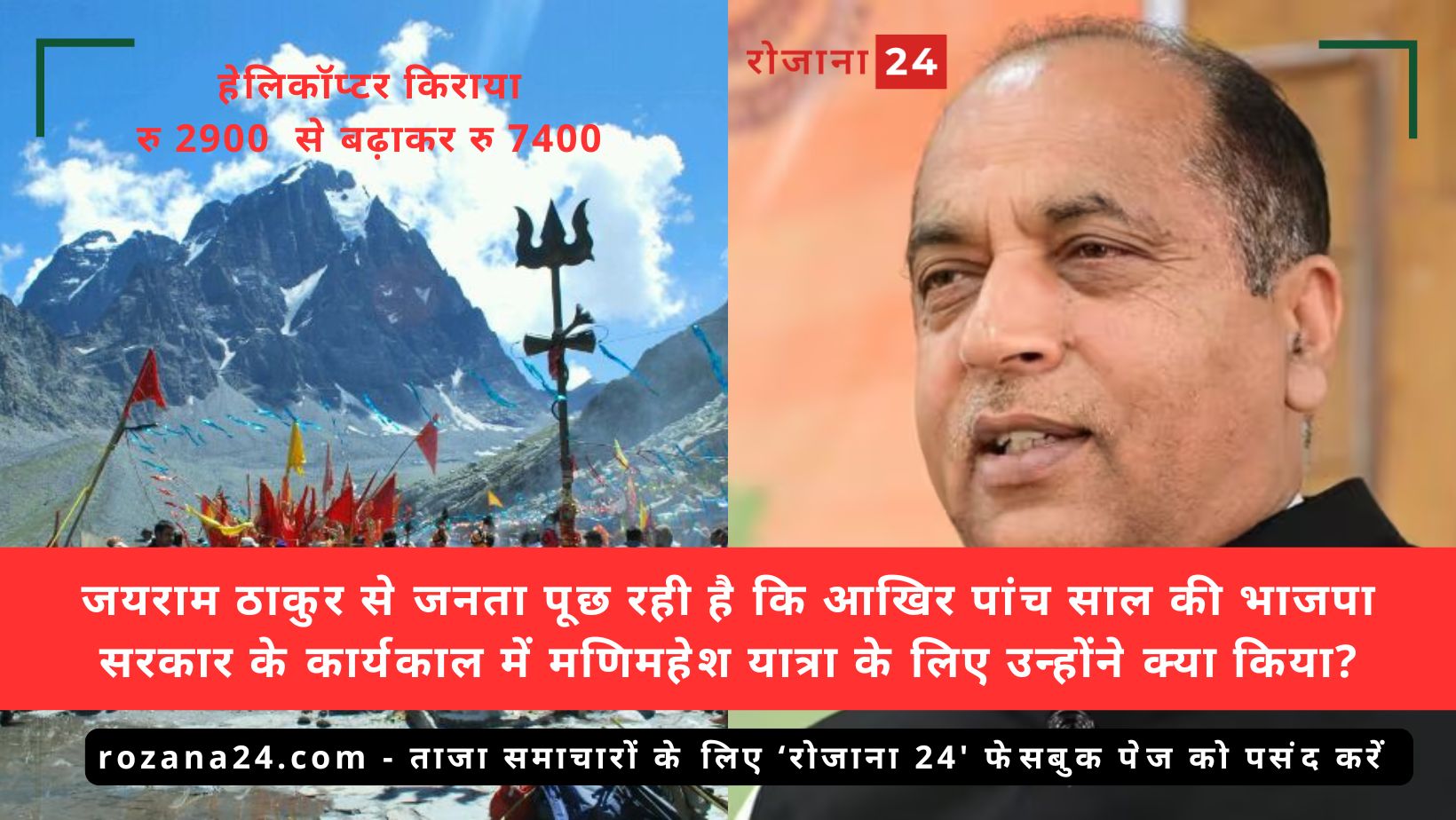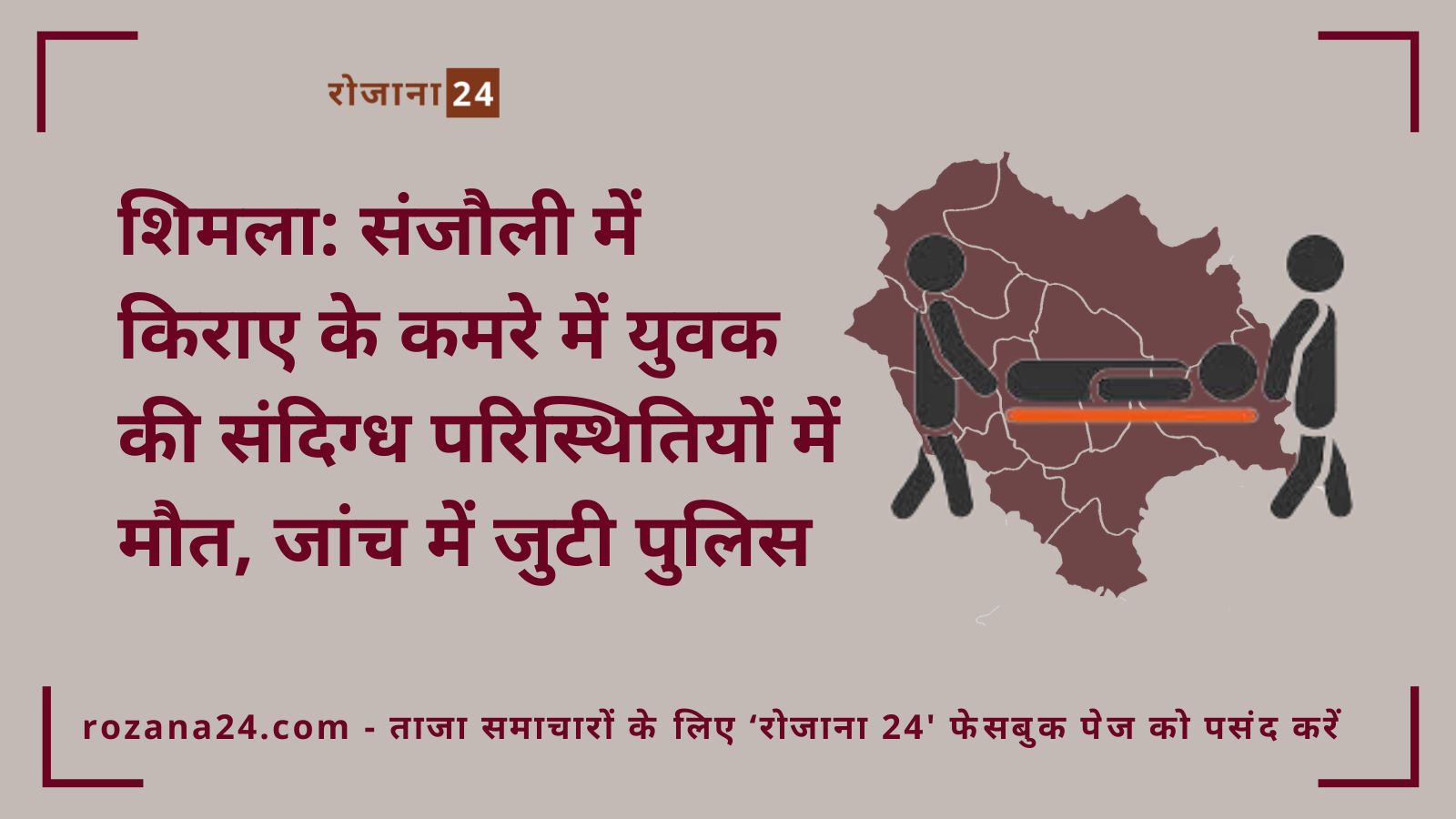टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) एक्ट को शहरी और ग्रामीण विकास को व्यवस्थित करने, अनियंत्रित निर्माण रोकने और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। हालांकि, यह कानून शहरी क्षेत्रों में फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन छोटे आदिवासी क्षेत्रों और गांवों में इसके प्रभावों को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं। इस कानून की कठोर नीतियां पारंपरिक और स्थानीय जरूरतों के अनुकूल नहीं होतीं, जिससे इन क्षेत्रों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
1. पारंपरिक स्वायत्तता की हानि
आदिवासी समुदाय और ग्रामीण पंचायतें पारंपरिक रूप से अपनी भूमि और निर्माण प्रथाओं का प्रबंधन अपने स्थानीय कानूनों और रीति-रिवाजों के अनुसार करती आई हैं। TCP एक्ट एक केंद्रीकृत ढांचा लागू करता है, जिससे ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता सीमित हो जाती है। इस कारण सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता है और स्थानीय लोगों की भागीदारी घट जाती है।
2. कठोर भूमि उपयोग नीति
TCP एक्ट के तहत भूमि को आवासीय, व्यावसायिक और कृषि जैसे विशिष्ट उपयोगों में वर्गीकृत किया जाता है। जबकि, आदिवासी समुदाय मिश्रित भूमि उपयोग की परंपरा का पालन करते हैं, जिसमें उनके घर, पशुपालन क्षेत्र और कृषि भूमि एक साथ मौजूद होते हैं। कठोर ज़ोनिंग नियम इस पारंपरिक जीवनशैली को बाधित करते हैं और ग्रामीणों को एक असंगत शहरी योजना के अनुरूप ढालने के लिए मजबूर करते हैं।
3. वित्तीय बोझ में वृद्धि
TCP एक्ट के तहत निर्माण कार्यों के लिए कई प्रकार के परमिट, फीस और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। छोटे आदिवासी क्षेत्रों में जहां लोग पारंपरिक निर्माण पद्धतियों पर निर्भर होते हैं, वहां ये अतिरिक्त खर्च एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। आर्किटेक्चरल प्लान, पर्यावरणीय मंजूरी और सरकारी स्वीकृतियों की जटिलता के कारण कई परिवार आवश्यक मरम्मत या विकास कार्यों को टालने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
4. पारंपरिक वास्तुकला और संस्कृति पर खतरा
आदिवासी क्षेत्रों में घर पारंपरिक रूप से लकड़ी, मिट्टी और पत्थर जैसी स्थानीय सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जो जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं। TCP एक्ट अक्सर आधुनिक भवन मानकों को अनिवार्य करता है, जिससे इन समुदायों को महंगे और अप्राकृतिक निर्माण सामग्रियों का उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इससे न केवल आर्थिक बोझ बढ़ता है, बल्कि स्थानीय वास्तुकला और सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में पड़ती है।
5. नौकरशाही में देरी और भ्रष्टाचार
TCP एक्ट के तहत किसी भी निर्माण या भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए कई सरकारी विभागों से मंजूरी लेनी पड़ती है। इससे प्रक्रियाओं में देरी होती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कम साक्षरता दर वाले आदिवासी समुदायों को जटिल कानूनी औपचारिकताओं को समझने में कठिनाई होती है, जिससे वे दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों के शिकार बन जाते हैं।
6. आर्थिक विकास में बाधा
आदिवासी गांवों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, हस्तशिल्प और लघु व्यवसायों पर निर्भर होती है। TCP एक्ट के तहत व्यावसायिक भूमि उपयोग और व्यापार परमिट पर सख्त नियम लागू होते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए छोटे व्यवसाय, होमस्टे या कुटीर उद्योग स्थापित करना कठिन हो जाता है। इससे रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और युवा पीढ़ी को रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है।
7. स्थानीय भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों की अनदेखी
हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां विशिष्ट होती हैं, जिसके लिए विशेष प्रकार की योजना की जरूरत होती है। TCP एक्ट के तहत लागू मानक शहरी नियोजन मॉडल इन क्षेत्रों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते। इससे कमजोर बुनियादी ढांचा विकसित होता है, जो भूस्खलन, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में असमर्थ होता है।
क्या समाधान हो सकता है?
TCP एक्ट की सख्त नीतियों के बजाय, स्थानीय स्वशासन और ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार देने की जरूरत है, ताकि वे अपनी पारंपरिक भूमि उपयोग प्रथाओं के अनुसार योजनाएं बना सकें। सरकार को आदिवासी समुदायों के लिए विशेष छूट और लचीली नीतियां लागू करनी चाहिए, जो उनकी संस्कृति, जीवनशैली और आर्थिक जरूरतों के अनुकूल हों।